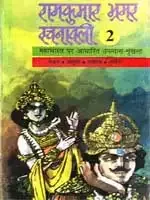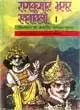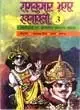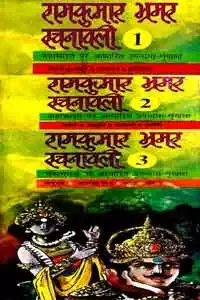|
बहुभागीय पुस्तकें >> रामकुमार भ्रमर रचनावली - खण्ड २ रामकुमार भ्रमर रचनावली - खण्ड २रामकुमार भ्रमर
|
105 पाठक हैं |
||||||
रामकुमार भ्रमर रचनावली एक बहुखण्डीय आयोजन है, जिसमें भ्रमरजी के बहुविध विधा-लेखन की उपलब्ध सभी रचनाओं के एकीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
धर्म क्या है और अधर्म कब, कहाँ, किस तरह हो जाता है ? यह एक ऐसा प्रश्न
है, जो युग-युगों से मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में विद्वानों,
ज्ञानियों और तपस्वियों के बीच चर्चा का विषय रहा हैं।
महाभारत के विभिन्न चरित्रों में युधिष्ठिर एक ऐसे
चरित्र हैं, जो सामान्य मनुष्य का जन्म पाकर धर्म और कर्म के बीच सन्तुलित
भाव से जीवन बिताने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक कर्म का
लेखा-जोखा धर्म की कसौटी पर करने की चेष्टा की है। समय–धर्म और
शाश्वत-धर्म के बीच सन्तुलन बनाये रखने के प्रयत्न किए हैं। वे ही हैं जो
धर्माधर्म को लेकर तत्कालीन विद्वानों और ज्ञानियों से बहुविध तर्क करते
हैं, जीवन–मूल्य खोजते हैं, सत्यासत्य के निर्धारण की चेष्टा
करते रहते हैं। इस सारी प्रकिया के बीच युधिष्ठिर ने संभवतः
गहरा कष्ट भोगा है। उनके शेष चारों भाई मुखर हैं। वे क्रोध, आवेश और
दुःख–सुख की अभिव्यक्ति अपने संवादों से अनेकानेक स्थानों पर कर
देते हैं। हर क्रिया, प्रतिक्रिया उनसे उत्तर पा लेती है, किन्तु
युधिष्ठिर सबसे अलग, शान्त–एक सीमा तक मौन पात्र हैं। कई-कई बार
तो लगता है कि युधिष्ठिर की यह शान्ति कहीं उनकी कायरता तो नहीं है ?
पर सच यह है कि युधिष्ठिर का मौन ही उनके सबसे अधिक पीड़ा भोगने का प्रमाण है। उनका जीवन ‘कौरव-पांडव कथा’ की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से तो जुड़ा है, किन्तु वह उस तरह घटनाप्रधान नहीं है, जिस तरह कर्ण, अर्जुन, दुर्योंधन आदि के चरित्र हैं... पहली बार में महसूस होता है कि युधिष्टिर केवल तर्कातर्क के चरित्र हैं, किन्तु गहरे पठन-पाठन के बाद लगता है कि युधिष्ठिर की चुप्पी ही उनकी अतिवेदना और वीरत्व हैं। वह किसी घटना से केवल प्रभावित होकर संवाद–भर की तात्कालिक प्रतिक्रिया देखकर मुक्ति नहीं पा सकते, अपितु उसे लेकर आत्मंथन का एक लम्बा दौर झेलते हैं.... यह झेलना कितना कष्टदायी है, कितना पीड़ाजनक या किस तरह छलनी कर डालने वाला-केवल युधिष्ठिर की ही तरह शान्त होकर सत्य की तहों तक पहुँचने वाले लोग जान सकते हैं। अपने समकक्ष चरित्रों की तुलना में युधिष्ठिर सबसे जटिल और सबसे सरल पात्र हैं। उनका ज्ञानमंथन उन्हें जटिल बनाता है, जबकि उनकी सत्यनिष्ठा उन्हें सरल बनाए रखती है। सरलता और जटिलता को एक साथ निबाहने की ये विलक्षण क्रिया ही उन्हें धर्मराज बनाती है।
पर सच यह है कि युधिष्ठिर का मौन ही उनके सबसे अधिक पीड़ा भोगने का प्रमाण है। उनका जीवन ‘कौरव-पांडव कथा’ की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से तो जुड़ा है, किन्तु वह उस तरह घटनाप्रधान नहीं है, जिस तरह कर्ण, अर्जुन, दुर्योंधन आदि के चरित्र हैं... पहली बार में महसूस होता है कि युधिष्टिर केवल तर्कातर्क के चरित्र हैं, किन्तु गहरे पठन-पाठन के बाद लगता है कि युधिष्ठिर की चुप्पी ही उनकी अतिवेदना और वीरत्व हैं। वह किसी घटना से केवल प्रभावित होकर संवाद–भर की तात्कालिक प्रतिक्रिया देखकर मुक्ति नहीं पा सकते, अपितु उसे लेकर आत्मंथन का एक लम्बा दौर झेलते हैं.... यह झेलना कितना कष्टदायी है, कितना पीड़ाजनक या किस तरह छलनी कर डालने वाला-केवल युधिष्ठिर की ही तरह शान्त होकर सत्य की तहों तक पहुँचने वाले लोग जान सकते हैं। अपने समकक्ष चरित्रों की तुलना में युधिष्ठिर सबसे जटिल और सबसे सरल पात्र हैं। उनका ज्ञानमंथन उन्हें जटिल बनाता है, जबकि उनकी सत्यनिष्ठा उन्हें सरल बनाए रखती है। सरलता और जटिलता को एक साथ निबाहने की ये विलक्षण क्रिया ही उन्हें धर्मराज बनाती है।
-राजकुमार भ्रमर
अग्रज
उन सबकी आँखें भय से फैली रह गई थीं। थरथराती पुतलियाँ दाँए-बाएँ घूमती और
रह-रहकर होंठ सूखने लगते। वे सभी शब्दहीन हो उठे थे। अपने भीतर एक खालीपन
महसूस करते हुए। लगता था कि महासागर की वीभत्सता ने उन्हें जीवनहीन कर
दिया हैं वे मात्र शरीर बनकर रह गए हैं। शरीर भी ऐसा जिसमें न गति है, न
शक्ति। कुछ खोखले पुतले हैं, जो रक्तसनी धरती पर दृष्टि–पार तक
बिखरी लाशों की फसल पर निगरानी कर रहे हैं।
इस बीच कितनी–कितनी बार उन्होंने एक–दूसरे को नहीं देखा होगा ? युधिष्ठिर ने सोचा फिर याद किया–बहुत बार !
किन्तु किसी भी बार, न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने उत्तर दिया। इसके बावजूद वे निरन्तर बोले हैं, निरन्तर प्रश्नोत्तर करते रहे हैं। प्रश्न इतने कि हर टूटे रथ, गिरी ध्वजा और क्षत–विक्षत हो चुकी लाश सिर्फ प्रश्न होकर रह गई है। सड़ती या सड़ चुकी लाशों से उठी दुर्गंध सवालों की एक बरखा बन गई है... आसमान में उड़ते-मँडराते गिद्धों, कौवों और अन्य मांसाहारी पक्षियों के झुंड़ काले बादलों की तरह उमड़-घुमड़कर धरती पर टूटते हुए... और उन सबके बीच जड़ पुतलों की तरह खड़े पाँचों भाई, अनेक साथी, शुभाकांक्षी और समर्थकों की एक भीड़ !
कुछ समय पूर्व सन्देशवाहक समाचार लाया था। कुरूराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का समाचार-‘‘प्रणाम महात्मन् ! नीतिज्ञ संजय ने कहा है कि दुःखी महाराज और महारानी पुत्रों-परिवारजनों की अन्तिम क्रिया करना चाहते हैं....’’
पत्थर की शिला जैसे खड़े रहे थे युधिष्ठिर। उनके इर्द-गिर्द भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व अन्य– सब उन्हीं की तरह शिला बने हुए। सुन रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं।
समझ रहे हैं, किन्तु सोचने की शक्ति नहीं।
आत्मबल जुटाकर युधिष्ठिर ने अपने-आपको संयत किया। मन हुआ था एक बार सन्देशवाहक से कहें- ‘‘जरा दोहराओ तो, तुमने क्या कहा था ?’’ किन्तु लगा यह इस तरह स्वंय को कुंठित बुद्धि और कमजोर साबित करेगें अतः बोले-‘‘अवश्य पधारें, किन्तु उसके पूर्व हम सब बंधु–बांधवों, परिचितों, गुरूजनों आदि के शव ढुँढ़वा रहे हैं- अच्छा होता कि कुलश्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट कुछ समय यही निवेदन किया था, धर्मराज पर महाराज और महारानी बहुत दुःखी हैं... इस समय उनकी इच्छा पूरी करना ही श्रेष्ठ है। मंत्री महोदय ने आपसे विशेष निवेदन करने को कहा है कि राजा-रानी के दुःख को इस समय किसी असुविधा के कारण न बढ़ने दें। यथासंभव उनकी इच्छापूर्ति करने में ही शुभ हैं। फिर यह भी देव कि महारानी के साथ वीर कौरवों की विधवाएँ भी अपने–अपने पतियों के अन्तिम दर्शन करना चाहती हैं।’’
एक गहरा श्वास लिया पांडु-पुत्र ने। बोले-‘‘ठीक है दूत ! उन्हें आने दो।’’ सन्देशवाहक चला गया। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर देखा, बोले-‘‘आओ, पूज्य धृतराष्ट्र के आगमन–पूर्व हम लोग बंधु–बांधवों और संबंधियों के शव खोजें।’’
अठारह दिन के क्रूरतम महायुद्ध को बीते हुए केवल दो दिन हुए थे। इन दिनों के भीतर–भीतर हजारों शव खोज, लिए गए थे जो दूर-दूरन्त मोर्चों पर कौरव-पांडव संग्राम के भीतर हत हुए। कोई शव ऐसा नहीं था, जिसे शरीर की पूर्णता में पाया गया हो। किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी का धड़, किसी–किसी के केवल सिर मिल सके और किसी का शरीर मिला, पर गला–सड़ा हुआ। शव खोजने वालों के हाथ–पैर यहाँ तक कि शरीर के अनेक हिस्से और वस्त्र लहू से रँग जाते... लाशों से उठती दुर्गध उन्हें बेसुधी के हाल तक ला छोड़ती। वे युद्ध में उतने नहीं थके थे, जितने इस संग्राम समाप्ति और पांडु-पुत्रों की जय के बाद वाली घिनौनी स्थिति में थकने लगे थे। अनेक योद्धाओं के शरीर बाणों से इस कदर बिंध गए थे कि उन्हें पहचानना कठिन हो चुका था। बहुतों की आँखें या शरीर के अन्य हिस्सों को गिद्धों ने नोचकर उन्हें कंकालों से भी कहीं अधिक वीभत्स और डरावना बना डाला था....
कुरूक्षेत्र के मैदान में ही नहीं उससे आगे-पीछे, सैकड़ों मील तक महासमर की विनाशलीला बिखरी थी और इस सबके परिणाम में हरे-भरे पौधों, फसलों, पेड़ों यहाँ तक कि पहाड़ियों में भी कालिख बिखर गई थी....जली लकड़ियों, झरे पत्तों तथा लहू की सूखी पत्तों–पपड़ियों से भरी भूमि देखने वाले का दिल दहला देती... पर अग्रज का आदेश था-‘‘बंधु-बांधवों की अन्त्य-क्रिया के लिए उन सभी के शव एक स्थान पर लाए जाने आवश्यक हैं !’’
अग्रज-युधिष्ठिर !
आदेशपालन में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और बची-खुची पांडव सेना के अनेक सैनिक या योद्धा जहाँ-तहाँ जा पहुँचे थे..... रणभूमि के उस भयानक श्मशान में शवों की खोज चल रही थी। लाशें खींचते हुए या जैसे-तैसे उठाए हुए उन्हें रथों पर डाला जाता, फिर सारथी उस रथ को गंगा किनारे की ओर ले जाता, जहाँ युधिष्ठिर, विदुर और कुन्ती उन्हें सिलसिलेवार रखवाते जाते।
कितने-कितने सम्बन्ध शव-स्थिति में नहीं पा लिए गए थे ? सैकड़ों। कोई किसी का बहनोई था, किसी का साला, किसी का पौत्र, किसी का पुत्र ,,,ऐसे जैसे इन्द्रधनुषी रंगों और हजारों आकार–प्रकारों की मणियों से मुक्त एक माला समूचा देश पहने हुए था और इस माला को उस देश के अपने ही हाथों से मूर्खतावश तोड़ डाला था.. सब मनके बिखर गए थे, सब टूट–फूट चुके थे, सब अपना व्यक्तित्व खो चुके थे।
जैसे-जैसे लाशों से लदे रथ चारों दिशाओं के मोर्चों से इस निश्चित स्थान पर आते जा रहे थे, वैसे–वैसे युधिष्ठिर को यही लग रहा था... सदा-सर्वदा, जीवन–संसार और व्यवहार पर बोलते रहे युधिष्ठिर सहसा चुप रहे थे... लगता था कि हर तर्क व्यर्थ हो गया है, हर सत्य धीमे-धीमें असत्य में बदलता हुआ और हर ज्ञानधारा दृश्य–सत्य की गरमी से सूखती, लुप्त होती हुई !
आकाश की और व्यग्र दृष्टि उठती और अकुलाया मन प्रश्न बनकर सूखे गले और तालू से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता-‘‘हे अनन्त ! कहाँ है मनुष्य का ज्ञान, विवेक, संवेदना और भावना ? सत्य क्या हैं और असत्य कौन-सा हैं ? किस प्राप्ति के लिए हम सब यह करते रहे हैं और किस अप्राप्ति के कारण यह सब हो गया हैं ?’’
किन्तु उत्तर नहीं।
उत्तर के नाम पर चीखते, गुर्राते और कर्ण कटु ध्वनियाँ निकालते हुए मांसाहारी पक्षियों का कलरव, पंखों की फड़फड़ाहटें और शवों की बढ़त के साथ-साथ उनका झुंडों में बदलते जाना !
युधिष्ठिर रथ खाली करवाते, शवों को क्रमबद्ध रखवाते, फिर चुपचाप एक ओर जा बैठते। प्रहरी कर दिए गए थे... वातावरण में क्रमशः दुर्गध सघन होती जा रही थी। यदा-कदा प्रहारियों का पंछियों पर चीखना, उन्हें शवों पर बैठने से पूर्व भगाने का प्रयत्न करना पांडु-पुत्र का ध्यान खींच लेता। एक क्षण के लिए विचारहीन होकर यांत्रिक ढंग से देखते रह जाते फिर गहरा श्वास लेकर अपने-आप में लौटते.... मन कभी व्यग्र नहीं होता था उनका। हर स्थिति, वातावरण, और व्यवस्था को अपने ज्ञान से वश में रखने का अद्भुत आत्मबल था उनके पास, किन्तु लगता था कि धर्माधर्म के इस युद्ध में यह तिरोहित हो गया है... उसकी जगह उभर आया है- ऐसा रिक्तता-बोध, जिससे न तो विवेक समझौता कर पाता है, न ज्ञान का कोई झोंका जिसे छू पाता है !
मन कहता-‘‘अपने-आपको संयत रखो अजातशत्रु ! तुम इस तरह निष्कर्षहीन तो कभी नहीं रहे ? तब एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने–आपको इस तरह व्यथित क्यों पाते हो ?’
‘‘हाँ, मैं स्वंय को संयत ही रखना चाहता हूँ...ये सगे–सम्बन्धी, बंधु–बांधव, सुख-दुख सभी कुछ भूल जाना चाहता हूँ... स्थितप्रज्ञ भाव से सब कुछ सहजता के साथ झेल जाना चाहता हूँ... किन्तु ?’’
यह किन्तु-उत्तरहीन !
इस किन्तु पर जय पाना होगा !
किस तरह पा सकेंगें ?
‘‘अपने ही भीतर सत्यासत्य का विवेचन करके।’’ लगा था कि बुद्धि और मन ने संयुक्त स्वर में कहा है- ‘‘वहीं एक मार्ग है‘! एकमात्र मार्ग !’’
लगा कि सिहर उठे हैं अपने इस आत्म-निर्देश से। इन आत्म-निर्देशों ने युधिष्ठिर को सदा ही सिहराये रखा है। थकाया है, नींद नहीं लेने ही है, कभी-कभी बेचैन कर दिया है।
क्या अब भी इस आत्म–निर्देश के वश होकर फिर से एक महासमर झेलेंगें ? हाँ ! सत्यासत्य का विवेचन किस महासमर से कम होता है ? लाखों–लाख अदृश्य घाव होते हैं।
मनबुद्धि पर, लाखों–लाख बार परम्पर आरोपों के प्रति–प्रहार ! यही सत्यास्य का विवेचन !
‘‘किन्तु अब तक महासमर ही तो लड़ते आए हैं युधिष्ठिर ! किसी बार अपने ही भाइयों के षड्यंत्रों से बचाव के लिए, किसी बार अधिकार की माँग के नाम पर और किसी बार युद्ध की विभीषिका न हो, इस प्रयत्न में ! और अन्त में यह महाविभीषिका से भरा घिनौना युद्ध !’’
युधिष्ठिर ने एक सिहरन महसूस की है... यह सिहरन युद्ध–परिणाम के कारण है या युद्ध के कारणों से– इस समय निश्चित कर पाना असंभव है ! पर सिहरन हुई है...
तीव्र दुर्गंध के कारण मन मितलियाँ–सी खाने लगा...अपने मन से हटकर दृश्य से जुड़ गए... कुछेक सैनिक नकुल की सहायता से शवों को रथ से उतार-उतारकर पंक्तिबद्ध लगा रहे थे..रहा नहीं गया था युधिष्ठिर पर। मितलियों पर काबू किया, अकुलाया चेहरा लिए हुए उनके पास जा पहुँचे।
‘‘भइया !’’ थकी, डूबती-सी आवाज में नकुल ने कहा था-‘‘दुःशासन का शव मिल गया है... देखो तो कितना वीभत्स लग रहा है !’’ नकुल की आँखों में जितनी पीड़ा थी, उससे कहीं ज्यादा भय और संभवतः उससे भी कहीं अधिक थरथराहट।
युधिष्ठिर बोल नहीं सके- भयभीत-से खड़े देखते रहे थे अपने कौरव बन्धु-को।
दुःशासन का शव वीभत्स स्थिति में उनके सामने पड़ा था। दुर्गंध के झोंके उगलता हुआ... मृत्यु–भय से आँखें फैली हुई थीं। चेहरे का काफी हिस्सा लहू से नहाया हुआ। उसी के साथ उसकी भुजा लटकी हुई थी.. सीने को बीच से फाड़ डाला था भीमसेन ने। उसमें से अंतडियाँ और मांस के लोथड़े बाहर आए थे।
सहसा याद हो आया था युधिष्ठिर को। उन्मत्त भीम ने दुःशासन की छाती फाड़कर दोनों हथेलियों की ओक में उसका लहू भरकर पिया था... कई अंजुलियाँ। क्रूरता और अमानवीयता से भरी इस हरकत को देखकर अनेक कौरव–पांडव सैनिक भाग खड़े हुए थे।
उत्तर नहीं दे सके थे युधिष्ठिर। बहुत लड़खड़ाते हुए अपने से ही तर्क करना चाहा था, समाधान भी ढूँढ़ लेने का प्रयत्न किया था। जी हुआ था, कह दें- ‘‘भीमसेन का वह कार्य अमानवीय तो अवश्य है किन्तु कारण उनकी दुर्दात प्रतिज्ञा है। दुःशासन की दुष्टताओं और षड़यंत्रों ने महाबली भीम को इतना आहत कर दिया था कि वह अपने भीतर की मनुष्यता, भावना और संवेदना को भूल गए।’’
पर लगा था कि उत्तर अपने ही भीतर रखे रहना होगा। अन्याय का परिष्कार अन्याय से होता है-यह तर्क देना अपने–आप में निर्लज्जतापूर्ण दुस्साहस से कम नहीं।
और दुःशासन की क्षत–विक्षत हो चुकी वीभत्स लाश उनके सामने है...
इस बीच कितनी–कितनी बार उन्होंने एक–दूसरे को नहीं देखा होगा ? युधिष्ठिर ने सोचा फिर याद किया–बहुत बार !
किन्तु किसी भी बार, न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने उत्तर दिया। इसके बावजूद वे निरन्तर बोले हैं, निरन्तर प्रश्नोत्तर करते रहे हैं। प्रश्न इतने कि हर टूटे रथ, गिरी ध्वजा और क्षत–विक्षत हो चुकी लाश सिर्फ प्रश्न होकर रह गई है। सड़ती या सड़ चुकी लाशों से उठी दुर्गंध सवालों की एक बरखा बन गई है... आसमान में उड़ते-मँडराते गिद्धों, कौवों और अन्य मांसाहारी पक्षियों के झुंड़ काले बादलों की तरह उमड़-घुमड़कर धरती पर टूटते हुए... और उन सबके बीच जड़ पुतलों की तरह खड़े पाँचों भाई, अनेक साथी, शुभाकांक्षी और समर्थकों की एक भीड़ !
कुछ समय पूर्व सन्देशवाहक समाचार लाया था। कुरूराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का समाचार-‘‘प्रणाम महात्मन् ! नीतिज्ञ संजय ने कहा है कि दुःखी महाराज और महारानी पुत्रों-परिवारजनों की अन्तिम क्रिया करना चाहते हैं....’’
पत्थर की शिला जैसे खड़े रहे थे युधिष्ठिर। उनके इर्द-गिर्द भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व अन्य– सब उन्हीं की तरह शिला बने हुए। सुन रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं।
समझ रहे हैं, किन्तु सोचने की शक्ति नहीं।
आत्मबल जुटाकर युधिष्ठिर ने अपने-आपको संयत किया। मन हुआ था एक बार सन्देशवाहक से कहें- ‘‘जरा दोहराओ तो, तुमने क्या कहा था ?’’ किन्तु लगा यह इस तरह स्वंय को कुंठित बुद्धि और कमजोर साबित करेगें अतः बोले-‘‘अवश्य पधारें, किन्तु उसके पूर्व हम सब बंधु–बांधवों, परिचितों, गुरूजनों आदि के शव ढुँढ़वा रहे हैं- अच्छा होता कि कुलश्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट कुछ समय यही निवेदन किया था, धर्मराज पर महाराज और महारानी बहुत दुःखी हैं... इस समय उनकी इच्छा पूरी करना ही श्रेष्ठ है। मंत्री महोदय ने आपसे विशेष निवेदन करने को कहा है कि राजा-रानी के दुःख को इस समय किसी असुविधा के कारण न बढ़ने दें। यथासंभव उनकी इच्छापूर्ति करने में ही शुभ हैं। फिर यह भी देव कि महारानी के साथ वीर कौरवों की विधवाएँ भी अपने–अपने पतियों के अन्तिम दर्शन करना चाहती हैं।’’
एक गहरा श्वास लिया पांडु-पुत्र ने। बोले-‘‘ठीक है दूत ! उन्हें आने दो।’’ सन्देशवाहक चला गया। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर देखा, बोले-‘‘आओ, पूज्य धृतराष्ट्र के आगमन–पूर्व हम लोग बंधु–बांधवों और संबंधियों के शव खोजें।’’
अठारह दिन के क्रूरतम महायुद्ध को बीते हुए केवल दो दिन हुए थे। इन दिनों के भीतर–भीतर हजारों शव खोज, लिए गए थे जो दूर-दूरन्त मोर्चों पर कौरव-पांडव संग्राम के भीतर हत हुए। कोई शव ऐसा नहीं था, जिसे शरीर की पूर्णता में पाया गया हो। किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी का धड़, किसी–किसी के केवल सिर मिल सके और किसी का शरीर मिला, पर गला–सड़ा हुआ। शव खोजने वालों के हाथ–पैर यहाँ तक कि शरीर के अनेक हिस्से और वस्त्र लहू से रँग जाते... लाशों से उठती दुर्गध उन्हें बेसुधी के हाल तक ला छोड़ती। वे युद्ध में उतने नहीं थके थे, जितने इस संग्राम समाप्ति और पांडु-पुत्रों की जय के बाद वाली घिनौनी स्थिति में थकने लगे थे। अनेक योद्धाओं के शरीर बाणों से इस कदर बिंध गए थे कि उन्हें पहचानना कठिन हो चुका था। बहुतों की आँखें या शरीर के अन्य हिस्सों को गिद्धों ने नोचकर उन्हें कंकालों से भी कहीं अधिक वीभत्स और डरावना बना डाला था....
कुरूक्षेत्र के मैदान में ही नहीं उससे आगे-पीछे, सैकड़ों मील तक महासमर की विनाशलीला बिखरी थी और इस सबके परिणाम में हरे-भरे पौधों, फसलों, पेड़ों यहाँ तक कि पहाड़ियों में भी कालिख बिखर गई थी....जली लकड़ियों, झरे पत्तों तथा लहू की सूखी पत्तों–पपड़ियों से भरी भूमि देखने वाले का दिल दहला देती... पर अग्रज का आदेश था-‘‘बंधु-बांधवों की अन्त्य-क्रिया के लिए उन सभी के शव एक स्थान पर लाए जाने आवश्यक हैं !’’
अग्रज-युधिष्ठिर !
आदेशपालन में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और बची-खुची पांडव सेना के अनेक सैनिक या योद्धा जहाँ-तहाँ जा पहुँचे थे..... रणभूमि के उस भयानक श्मशान में शवों की खोज चल रही थी। लाशें खींचते हुए या जैसे-तैसे उठाए हुए उन्हें रथों पर डाला जाता, फिर सारथी उस रथ को गंगा किनारे की ओर ले जाता, जहाँ युधिष्ठिर, विदुर और कुन्ती उन्हें सिलसिलेवार रखवाते जाते।
कितने-कितने सम्बन्ध शव-स्थिति में नहीं पा लिए गए थे ? सैकड़ों। कोई किसी का बहनोई था, किसी का साला, किसी का पौत्र, किसी का पुत्र ,,,ऐसे जैसे इन्द्रधनुषी रंगों और हजारों आकार–प्रकारों की मणियों से मुक्त एक माला समूचा देश पहने हुए था और इस माला को उस देश के अपने ही हाथों से मूर्खतावश तोड़ डाला था.. सब मनके बिखर गए थे, सब टूट–फूट चुके थे, सब अपना व्यक्तित्व खो चुके थे।
जैसे-जैसे लाशों से लदे रथ चारों दिशाओं के मोर्चों से इस निश्चित स्थान पर आते जा रहे थे, वैसे–वैसे युधिष्ठिर को यही लग रहा था... सदा-सर्वदा, जीवन–संसार और व्यवहार पर बोलते रहे युधिष्ठिर सहसा चुप रहे थे... लगता था कि हर तर्क व्यर्थ हो गया है, हर सत्य धीमे-धीमें असत्य में बदलता हुआ और हर ज्ञानधारा दृश्य–सत्य की गरमी से सूखती, लुप्त होती हुई !
आकाश की और व्यग्र दृष्टि उठती और अकुलाया मन प्रश्न बनकर सूखे गले और तालू से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता-‘‘हे अनन्त ! कहाँ है मनुष्य का ज्ञान, विवेक, संवेदना और भावना ? सत्य क्या हैं और असत्य कौन-सा हैं ? किस प्राप्ति के लिए हम सब यह करते रहे हैं और किस अप्राप्ति के कारण यह सब हो गया हैं ?’’
किन्तु उत्तर नहीं।
उत्तर के नाम पर चीखते, गुर्राते और कर्ण कटु ध्वनियाँ निकालते हुए मांसाहारी पक्षियों का कलरव, पंखों की फड़फड़ाहटें और शवों की बढ़त के साथ-साथ उनका झुंडों में बदलते जाना !
युधिष्ठिर रथ खाली करवाते, शवों को क्रमबद्ध रखवाते, फिर चुपचाप एक ओर जा बैठते। प्रहरी कर दिए गए थे... वातावरण में क्रमशः दुर्गध सघन होती जा रही थी। यदा-कदा प्रहारियों का पंछियों पर चीखना, उन्हें शवों पर बैठने से पूर्व भगाने का प्रयत्न करना पांडु-पुत्र का ध्यान खींच लेता। एक क्षण के लिए विचारहीन होकर यांत्रिक ढंग से देखते रह जाते फिर गहरा श्वास लेकर अपने-आप में लौटते.... मन कभी व्यग्र नहीं होता था उनका। हर स्थिति, वातावरण, और व्यवस्था को अपने ज्ञान से वश में रखने का अद्भुत आत्मबल था उनके पास, किन्तु लगता था कि धर्माधर्म के इस युद्ध में यह तिरोहित हो गया है... उसकी जगह उभर आया है- ऐसा रिक्तता-बोध, जिससे न तो विवेक समझौता कर पाता है, न ज्ञान का कोई झोंका जिसे छू पाता है !
मन कहता-‘‘अपने-आपको संयत रखो अजातशत्रु ! तुम इस तरह निष्कर्षहीन तो कभी नहीं रहे ? तब एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने–आपको इस तरह व्यथित क्यों पाते हो ?’
‘‘हाँ, मैं स्वंय को संयत ही रखना चाहता हूँ...ये सगे–सम्बन्धी, बंधु–बांधव, सुख-दुख सभी कुछ भूल जाना चाहता हूँ... स्थितप्रज्ञ भाव से सब कुछ सहजता के साथ झेल जाना चाहता हूँ... किन्तु ?’’
यह किन्तु-उत्तरहीन !
इस किन्तु पर जय पाना होगा !
किस तरह पा सकेंगें ?
‘‘अपने ही भीतर सत्यासत्य का विवेचन करके।’’ लगा था कि बुद्धि और मन ने संयुक्त स्वर में कहा है- ‘‘वहीं एक मार्ग है‘! एकमात्र मार्ग !’’
लगा कि सिहर उठे हैं अपने इस आत्म-निर्देश से। इन आत्म-निर्देशों ने युधिष्ठिर को सदा ही सिहराये रखा है। थकाया है, नींद नहीं लेने ही है, कभी-कभी बेचैन कर दिया है।
क्या अब भी इस आत्म–निर्देश के वश होकर फिर से एक महासमर झेलेंगें ? हाँ ! सत्यासत्य का विवेचन किस महासमर से कम होता है ? लाखों–लाख अदृश्य घाव होते हैं।
मनबुद्धि पर, लाखों–लाख बार परम्पर आरोपों के प्रति–प्रहार ! यही सत्यास्य का विवेचन !
‘‘किन्तु अब तक महासमर ही तो लड़ते आए हैं युधिष्ठिर ! किसी बार अपने ही भाइयों के षड्यंत्रों से बचाव के लिए, किसी बार अधिकार की माँग के नाम पर और किसी बार युद्ध की विभीषिका न हो, इस प्रयत्न में ! और अन्त में यह महाविभीषिका से भरा घिनौना युद्ध !’’
युधिष्ठिर ने एक सिहरन महसूस की है... यह सिहरन युद्ध–परिणाम के कारण है या युद्ध के कारणों से– इस समय निश्चित कर पाना असंभव है ! पर सिहरन हुई है...
तीव्र दुर्गंध के कारण मन मितलियाँ–सी खाने लगा...अपने मन से हटकर दृश्य से जुड़ गए... कुछेक सैनिक नकुल की सहायता से शवों को रथ से उतार-उतारकर पंक्तिबद्ध लगा रहे थे..रहा नहीं गया था युधिष्ठिर पर। मितलियों पर काबू किया, अकुलाया चेहरा लिए हुए उनके पास जा पहुँचे।
‘‘भइया !’’ थकी, डूबती-सी आवाज में नकुल ने कहा था-‘‘दुःशासन का शव मिल गया है... देखो तो कितना वीभत्स लग रहा है !’’ नकुल की आँखों में जितनी पीड़ा थी, उससे कहीं ज्यादा भय और संभवतः उससे भी कहीं अधिक थरथराहट।
युधिष्ठिर बोल नहीं सके- भयभीत-से खड़े देखते रहे थे अपने कौरव बन्धु-को।
दुःशासन का शव वीभत्स स्थिति में उनके सामने पड़ा था। दुर्गंध के झोंके उगलता हुआ... मृत्यु–भय से आँखें फैली हुई थीं। चेहरे का काफी हिस्सा लहू से नहाया हुआ। उसी के साथ उसकी भुजा लटकी हुई थी.. सीने को बीच से फाड़ डाला था भीमसेन ने। उसमें से अंतडियाँ और मांस के लोथड़े बाहर आए थे।
सहसा याद हो आया था युधिष्ठिर को। उन्मत्त भीम ने दुःशासन की छाती फाड़कर दोनों हथेलियों की ओक में उसका लहू भरकर पिया था... कई अंजुलियाँ। क्रूरता और अमानवीयता से भरी इस हरकत को देखकर अनेक कौरव–पांडव सैनिक भाग खड़े हुए थे।
उत्तर नहीं दे सके थे युधिष्ठिर। बहुत लड़खड़ाते हुए अपने से ही तर्क करना चाहा था, समाधान भी ढूँढ़ लेने का प्रयत्न किया था। जी हुआ था, कह दें- ‘‘भीमसेन का वह कार्य अमानवीय तो अवश्य है किन्तु कारण उनकी दुर्दात प्रतिज्ञा है। दुःशासन की दुष्टताओं और षड़यंत्रों ने महाबली भीम को इतना आहत कर दिया था कि वह अपने भीतर की मनुष्यता, भावना और संवेदना को भूल गए।’’
पर लगा था कि उत्तर अपने ही भीतर रखे रहना होगा। अन्याय का परिष्कार अन्याय से होता है-यह तर्क देना अपने–आप में निर्लज्जतापूर्ण दुस्साहस से कम नहीं।
और दुःशासन की क्षत–विक्षत हो चुकी वीभत्स लाश उनके सामने है...
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book